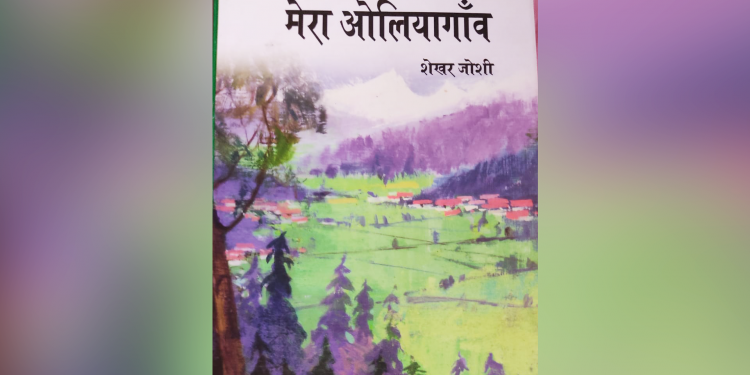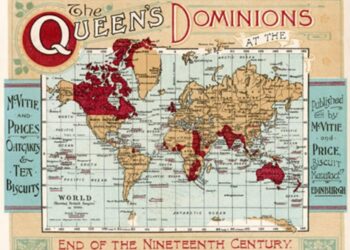महेश दर्पण ने पढ़ ली है पुस्तक ‘मेरा ओलियागांव’. उनकी नजर से आप भी पढ़िए…
इधर के स्मृति आख्यानों में प्रायः यह पाया गया है कि लेखक विवरणों में रस लेने लगा और मितकथन का महत्व ही बिसरा गया। किंतु हाल ही में प्रकाशित शेखर जोशी की पुस्तक ‘मेरा ओलियागांव’ में यह कमज़ोरी आदि से अंत तक कहीं नज़र नहीं आती। उनका यह ग्रामवृत्त इस दृष्टि से स्मृतियों की ऐसी भोली प्रस्तुति है, जहां लेखक का बाल-मन रह-रह कर सचेत हो उठता है। लेखक की ओर से अपने ग्रामीण परिवेश की स्मृति में यह रचनात्मक रूप में भूमि ऋण अदा करने जैसा ही कहा जा सकता है। शेखर जी अपने ओलियागांव के प्रति प्रारंभ में ही ‘नमन’ शीर्षक कविता से विनत हैं। इसके माध्यम से वह अपने पाठकों को भी उनके भीतर पालथी मार कर बैठे उस बच्चे की याद दिला देते हैं, जिसे वे कभी बहुत पीछे छोड़ आए होंगे।
पुस्तक से पता चलता है कि झिझाड़ के कुछ परिवारों ने एक समय ओलियागांव जैसे सुरम्य स्थान की खोज की और वहीं बस गये। यह स्थान काठगोदाम-गरुड़ मोटर मार्ग पर मनाड़ और सोमेश्वर के बीच स्थित रनमन से आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बालपन की स्मृतियों में कैसा था भला यह गांव? यहां पाई जाने वाली चिड़ियों के प्रकार, बुरूंश की आभा, स्यूंत का स्वाद, आलूबुखारा, नाशपाती, किलमोड़ा, घिंघारु, सेब का आनंद और भुट्टे की पंक्तियां गिनना, कौओं के लिए विशेष त्यौहार घुघुती, प्राकृतिक सौंदर्य और धूप का घड़ी बन जाना अलग ही किस्म का अनुभव पढ़ना है। जंगल में आग पर काबू पाना और मैदानी चीजों के प्रति आश्चर्य भरी नज़र से देखना, चाहे वह तरबूज़ हो, सुराही या फिर रेल। भोलेपन में विश्वास का आलम यह कि रक्षा और कष्टनिवारण के लिए जागर का प्रावधान। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करना और आशीर्वादस्वरूप ‘शतंजीवी भव’ सुनना। सरल आक्रोश में दूसरे को सबक सिखाने के लिए खुद भले ही कितना कष्ट उठाना पड़ जाए, कोई परवाह नहीं। व्यक्ति हों, वनस्पति या वस्तुएं, सभी ध्यान खींचते हैं। इस स्मृति आख्यान में प्रथम विश्वयुद्ध से लौटे और उपलब्धियां पाने वाले दो सैनिक भी हैं, याक की खाल का पिटारा है, कस्तूरी मृग के बालों की मसनद, तिब्बती गाय की पूंछ के बालों के चंवर और थुलमा भी।
यही नहीं, विकास के बाद जो बचा नहीं रह गया, उसे भी लेखक ने बड़े भावुक मन से स्मरण किया है, जैसे वह एकाकी देवदारु। पर वह समय था स्वतंत्रता संग्राम का चरम। गांधी, गांधीवादी और वंदेमातरम् तथा देशभक्ति की प्रार्थनाएं। इन सब में ओलियागांव वाले बढ़-चढ़कर भाग भले न ले रहे हों, तटस्थ भी तो न थे।
परिवेश और समय के साथ ही शेखर जोशी अपने बारे में भी बहुत कुछ आत्मीय किस्से के अंदाज़ में सुनाते नज़र आते हैं। इसी ओलियागांव में दामोदर जोशी और हरिप्रिया की संतान के रूप में 10 सितंबर, 1932 को लेखक का जन्म हुआ। पुरोहित से नाम मिला- चंद्रदत्त, किंतु जब 1944 में स्कूल में नाम लिखाया तो मामा ने उसे चंद्रशेखर में परिवर्तित करा दिया। यही बाद में शेखर जोशी हुआ।
इस शेखर का बचपन खेती में आनंद लेते, धान रोपाई और अखोड़झडै़ का उत्सव देखते, धान की खुशबू लेते, शैतानियां करते, गिरि खेलते और कृषक संस्कृति में पलते बीता। यहां बैल, गोबर, गोमूत्र, चटाई, गेहूं की सुरक्षा के उपाय, फलते फलों की ओर संकेत की तहज़ीब सीखते, दाड़िम के फूलों से खेलते और बेटा-बेटी में भेद को करीब से देखते समय की स्मृतियों को बड़े मार्मिक किंतु तटस्थ ढंग से उकेरा है लेखक ने। पशु-पक्षियों से मनुष्य के सम्बंधों के बीच गोधूलि दृश्य की गहरी संगीतमय स्मृति के साथ नमक का पानी मिलाकर गाय की नाक से जौं निकालना किसी यादगार दृश्य की तरह साथ हो लेता है। पहाड़ में बाघों का आतंक कितना भयावह होता है, यह इसी से जाना जा सकता है कि घर से केवल बीस कदम की दूरी पर बाधों द्वारा अनेक जीवों की हत्या के बाद बाघों के संहार का इंतजाम करना भी गांव वालों के लिए आम बात रही। ऐसी घटनाओं समेत प्रकृति का आत्मीय चित्रण रस्किन बाँड के लेखन की स्मृति दिला देता है। पर इसी सबके साथ वात-पीड़ा के निवारण के लिए कटोरे में रखी बाघ की चर्बी को मक्खन समझ कर कथानायक द्वारा खा लेना और बेस्वाद पाना भी एक रोचक प्रसंग है। जीवित ही नहीं, मृत बाघ की खाल भी कैसे बच्चों के लिए कौतुक और कुत्तों के लिए आतंक का कारण बन जाती है, यह बताते हुए शेखर जोशी पाठक को किसी और ही दुनिया में खींच ले जाते हैं।
‘मेरा ओलियागांव’ में एक तरह से इस परिवेश का पूरा चरित्र उतर आता है। एक अर्थ में तो यहां अतीत पुनजीर्वित हो जाता है। कहने को यह एक शांत स्थान रहा है, जहां कभी कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता था, बस सामान्य अनबन हुआ करती जो फिर जल्द ही ठीक भी हो जाती। किंतु निचली सतह में उतर कर देखें, तो मूल चरित्र में यह एक सामंती आधिपत्य का गांव रहा है। भू-स्वामियों का कामगरों के साथ बर्ताव और मेहनताने के रूप में उन्हें अन्न देते हुए भी एकाध काम करने को और बता देना जैसे उनका अधिकार ही रहा। पुरुषों के लिए अतिरिक्त उदार इस समाज मंे स्त्रियां घरों में उपेक्षिता का सा जीवन जीने को विवश रहीं। वे मनचाहा कर सकने को भी स्वतंत्र नहीं थीं। लेखक की भाषा में यह स्वप्नभंग की उदासी जैसी थी। ऐसे माहौल में उनके जीवन में संगीत की एक प्रेरक भूमिका रहती। पर्व-त्यौहार उनके लिए कलात्मक प्रतिभा के विकास के अवसर जुटाते। एपण बनाती लड़कियां क्रमशः अपनी सीमा में रहकर कला से प्रेम करना सीखती जातीं। पर जीना उन्हें दुभांत में ही पड़ता, क्योंकि कक्षा चार के बाद उनके लिए स्कूल की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसे में स्वयं को घरेलू कामों में व्यस्त कर लेने के अतिरिक्त फिर कोई चारा रह भी नहीं जाता। महिलाओं का इलाज डाम द्वारा किया जाना भी पारंपरिक रूप मंे चला आ रहा था, पर इन महिलाओं की उदारता देखिए, घर में किसी के अस्वस्थ हो जाने पर पूजा में उचैण रख आतीं और ईश्वर से प्रार्थना करतीं कि वह जल्द ठीक हो जाए। लेखक ने दैनिक जीवन के खान-पान और छुआछूत से जुड़े कड़े नियमों के साथ उस व्यवहारकुशलता को भी सामने रखा है जो समय पड़ने पर इस्तेमाल कर ली जाती थी। समाज ने उन लोगों को अछूत बना रखा था, जो उसके सबसे अधिक काम आते थे। इनमें कारीगर, लोहार, राजगीर, बढ़ई, हलवाहा, तेली, ढोली, बारुड़ी, ठठेरे आदि आते थे। इनका स्पर्श तक वर्जित था। उन्हें हर तरह के अपमान में जीने की आदत डालनी होती थी।
ग्रामीण जीवन का अनुशासन, पूजा-पाठ, इष्टदेव पैथल जी के मंदिर में घंटियां और उनमें अंकित जानकारी, बाल-प्रार्थनाएं, अंधविश्वास, छल लगना, भभूत से सुरक्षा और पेड़ों तले पढ़ाई ही नहीं, तिब्बत से हुणियों का आगमन व जम्बू, हींग, गंघ्रैणी, मूंग, शिलाजीत, कस्तूरी सहित अनेक जड़ी-बूटी बेचना और बच्चों के भय का निवारण तक एक-एक चीज इन स्मृतियों का हिस्सा बड़ी सहजता से बनी है। अपने मूल्यों और विश्वास का आलम यह कि वैद्य हरिकृष्ण पांडेय को चांदी का सिक्का इसलिए जबरन दिया जाता ताकि दवाएं असर अवश्य करें।
कल्पना कीजिए, कैसा होगा खबरों और मनोरंजन से कटा वह समाज, जहां किसी के पास रेडियो तक नहीं था। अल्मोड़ा से अखबार ‘शक्ति’ आता, वह भी केवल ताऊ जी के यहां। पर मस्ती ऐसी कि होली की बैठक के साथ याद रह जाए बाबू का स्वांग, रामलीला, यज्ञोपवीत, हरेला, जन्माष्टमी का पट्टा, पूजा के बर्तनों को खट्टी घास से चमकाना, बुनाई, रक्षाबंधन की जगह जनेऊ पूर्णिमा, ओलुग संक्रान्ति और सोमेश्वर मेला। कुल मिलाकर यह सब एक ऐसे समाज की सृष्टि करता है, जो बस अपने में जीता था। प्रधान की भूमिका और फौती रजिस्टर ही नहीं, छोटी बावड़ी में दीवार का पर्दा और स्त्री-पुरुषों का अलग-अलग स्नान, बोन चाइना क्राॅकरी के बारे में भ्रांति और कौतुक का भाव भी इस ग्रामीण परिवेश की स्मृतियों को दिलचस्प बनाते हैं। त्रिलोचन ताऊ जी और उनकी दूरबीन, मोतीराम दादा जी के नींबू, और लीलाधर ताऊ जी का वह मार्मिक प्रसंग जिसमें रात के आठ-नौ बजे भी कराह सुनकर पूरे एक किलोमीटर मशाल लेकर जाना और अपरिचित बुजुर्ग को पीठ पर लाद कर घर लाना ही नहीं, खुद पकाकर खाना खिलाना भी एक अविस्मरणीय प्रसंग है। हैरानी बस इस बात की है कि शेखर जी उस नारे का उल्लेख नहीं करते जो उनके लीलाधर ताऊजी फागुन की मस्ती में, खेत पर काम करती महिलाओं को देख कर लगाने को कहा करते थे। जाने क्या रहा होगा वह नारा जो ताऊ जी को उन्मुक्त कर देता था!
इस स्मृति आख्यान में स्वयं को अन्वेषित करने का तो सात्विक प्रयास है ही, किस्सों ऊपर किस्से चले आते हैं और पाठक को अपने प्रवाह में बहाते चलते हैं। ऐसा ही रोचक किस्सा है दुर्गादत्त जैसे जानकार का जर्मन विद्वान को लोकसंस्कृति का पाठ पढ़ाने का। शेखर जी का कथाकार यहां चरित्रों की एक चमक भरी झलक देकर आगे बढ़ लेता है, उनके मोह में फंसा नहीं रह जाता। हां, इसी क्रम में वह असंतोषी, विघ्नसंतोषी व दयाकांक्षी चरित्रों का प्रभावी स्केच भी खींच देता है।
शेखर जोशी जैसे बड़े कथाकार का यह आत्मवृत्त उनके परिवार के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रथम पुरुष में देता है। बताता है कि दादा-दादी का निधन तभी हो गया था जब इनके पिता केवल नौ बरस के थे। प्यार मिला इन्हें ननिहाल-बिसाड़ागांव, पिथौरागढ़ में। पिता बयालीस बरस की उम्र में ही विधुर हो गए। अपनी मां की स्मृति शेखर के मन में बस एक नारी आकृति की रही। दुखद प्रसंग यह कि मां की मृत्यु प्रसव-काल में डाक्टरी सुविधा न मिलने से हुई। पिता करिश्माई दिमाग के उद्योगशील व प्रयोगधर्मी कैसे थे, इसके प्रमाण-प्रसंग तो इस कथा में आते ही हैं, पद्मादत्त ताऊ जी के प्रयोग भी कम रोचक नहीं। अपनी बाल-शैतानियों को भी लेखक ने खुलकर सामने रखा है, जिसमें अधन्नियां गायब कर बीड़ी-सिगरेट पीना और बदबू दूर करने के लिए घिंगारू के दाने व पत्ते चबा लेना भी शामिल है। यह उस दुनिया के बच्चे की दास्तान है जिसमें उसे बिस्कुट और नारंगी गोली भी एक बड़ा आकर्षण लगता रहा।
स्थानीय रंगत के साथ ही यहां देसज अंदाज में बनती और खुलती भाषा का मज़ा भी देखने को मिलता है। बुलबुलीबाज, साबुणेन, कनफंुकवा, स्वगत भाषण करते बुजुर्ग की मेडिकल रिपोर्ट और रामदत्त ताऊजी की भाषा मंे बनते शब्दों का मज़ा, जहां विरोध सूचक ‘रनकर’ हो या बेचारा का बोध कराने वाला ‘रांडो’ बन जाता हो। पनुवा लोहार की कलयुगी रामायण सुनाने का अपना अंदाज़ हो या लीलाधर ताऊजी की कूट भाषा का खेल, अनेक वक्ताओं के बोलने को गौर से सुनना हो या विलोमकथन की शक्ति को पहचानना, ठहरी हुई जिंदगी में यह सब उत्साह उत्पन्न करने वाले उपादान अवश्य रहे होंगे।
इस परिवेश से उठकर, बाद में अपनी हैसियत एक प्रेरक लेखक की बना लेने वाले शेखर जोशी को बहुत कुछ अपने इस समय से भी मिला है। पुस्तक यह संकेत देती है कि शेखर जी की कहानी ‘व्यतीत’ में जड़ों से विस्थापित वृद्ध और कोई नहीं, बाबू ही हैं। बचपन में जिस चंद्रशेखर को भजन गाता देख उसके जोगी हो जाने की आशंका मां में जगी थी, तब वह यह न समझ पाई होंगी कि यही बच्चा रामदत्त ताऊ जी के बात करने के ढंग को भी गौर से देख-सुन रहा है, इसी सबके बीच उसे लेखन के सूत्र भी मिलते जा रहे होंगे- ‘‘ताऊ जी का बात करने का ढंग अनूठा था। वह किसी एक विषय को लेकर बात शुरू करते, तो थोड़ी देर बाद उस विषय से सम्बन्धित किसी अन्य प्रसंग पर बतियाने लगते। फिर शाखाएं फूटती चली जातीं और मूल प्रसंग पीछे छूट जाता। पर प्रत्येक नए प्रसंग में कुछ-न-कुछ रोचकता बनी रहती। मेरा कथाकार मन इन बातों में नए-नए सूत्र पाता जा रहा था। मैं घंटों तक उनकी बातें मन लगाकर सुनता रहा…।’’ यह प्रक्रिया एक धैर्यवान श्रोता बनकर बहुत कुछ सीखने और जानने की रही होगी। साथ ही यह भाव भी कि इन अनुभवों का लाभ दूसरे भी उठायें।
अपने साहित्यरसिक मन पर पड़ने वाले प्रारंभिक प्रभावों में शेखर जी सुमित्रानंदन पंत की कृति ‘उच्छवास’ के नाद सौंदर्य को भी देते हैं जिससे वह अभिभूत रहते थे। वैसे लेखक में काव्य रुचि जागृत करने में ‘गोपी-गीत’ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जरूर उन्हें मंझले मामा लिखित ‘ब्रह्मसूत्र’ की टीका के खण्डों में प्रकाशित उनका नाम देखकर संभवतः लेखक बनने की इच्छा जागृत हुई होगी। इस पुस्तक के नायक को बागेश्वर मेले में भी ग्रामीण आशुकवियों की वाग्विलास भरी रचनाएं सुनकर भी बहुत कुछ रुचा होगा। जीवन की इन सत्य घटनाओं में से कुछ, अनुभव के स्तर पर बहुत कुछ स्मरणीय दे जाती हैं। जैसे रणबांकुरे फौजी को विदा करने बस तक आई महिलाओं का रुदन और उन सैनिकों में बहुत कम का सकुशल लौटना लेखक के मन पर ऐसा बैठ गया कि फिर उसकी पहली कहानी ‘राजे खत्म हो गए’ इसी तरह के प्रसंग पर लिखी गई। यह एक फौजी की वृद्धा मां पर लिखी रचना है। लेखक की मान्यता है कि संभवतः ‘कोसी का घटवार’ कहानी का नायक गुसाईं भी इसी तरह की घटना का परिणाम हो।
अपने आसपास के लोग, जीवन और प्रेरणाएं कैसे एक रचनाकार के लिए चरित्रों और कथानकों के बीज बन जाते हैं, यह इस गांव में ही नहीं, उससे बाहर निकलकर भी शेखर जोशी के संदर्भ में सही प्रतीत होता है। उनकी कहानियांे में ‘उस्ताद’, ‘मेंटल’ या ‘आशीर्वचन’ पढ़ते हुए यह महसूसा जा सकता है। बालपन में यह लेखक भले ही सामंती संस्कारों में पला, किंतु उसके आगामी जीवन-संघर्ष ने उसे बहुत कुछ सिखाया। वह प्रारंभिक संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर निकल एक स्वस्थ समाज का विवेकशील नागरिक बना। आज नवें दशक के उत्तरार्ध में भी शेखर जोशी का स्मृतिकार इन स्मृतियों को इस प्रकार सजीव कर गया है कि यह स्मृति आलेख आज के युवा रचनाकारों के लिए प्रकाशस्तंभ ही बन गया है।
मेरा ओलियागांव: शेखर जोशी
मूल्यः 190 रुपये
प्रकाशकः नवारुण, गाजियाबाद-201012 (उत्तर प्रदेश)
वरिष्ठ कथाकार महेश दर्पण के सात कहानी संग्रह, एक यात्रा वृत्तांत, पांच जीवनवृत्त और कई अन्य विधाओं में पुस्तकें आ चुकी हैं. कन्नड़ उर्दू, पंजाबी, मलयाली और रूसी भाषा में रचनाओं का अनुवाद हो चुका है. उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है.